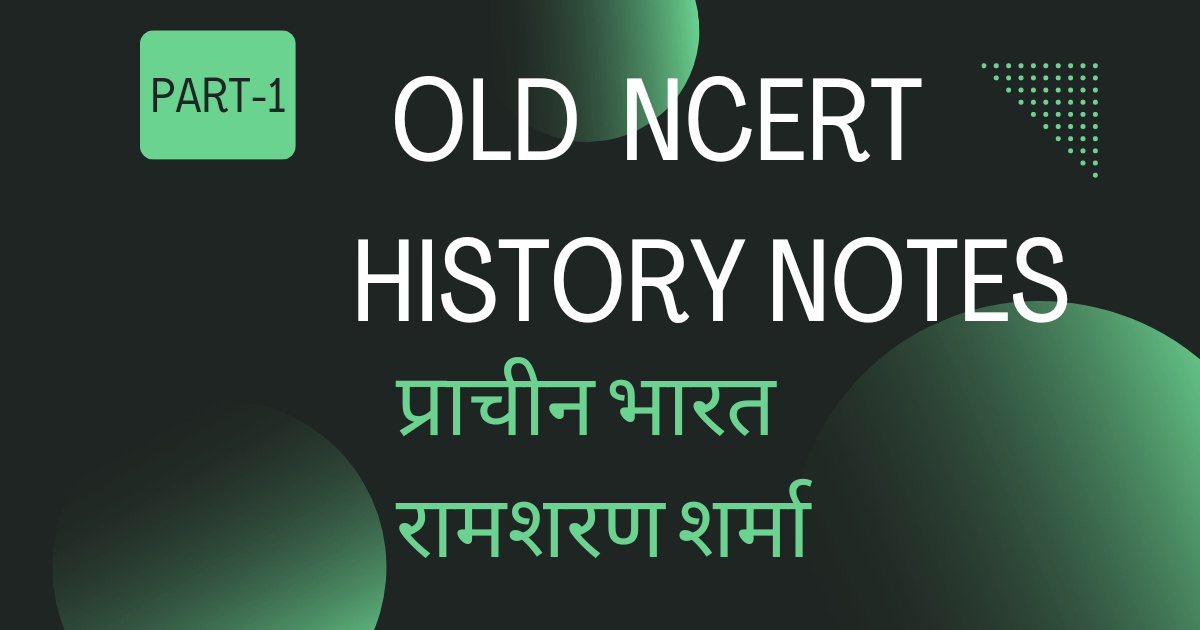यहाँ आपके लिए “Old NCERT R S Sharma: Ancient History” के अध्याय 1 “प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्त्व” के विस्तृत नोट्स तैयार किए गए हैं, जो UPSC परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे।
प्राचीन भारत (रामशरण शर्मा)
| 1. | प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्त्व |
| 2. | प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक |
| 3. | स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण |
| 4. | भौगोलिक ढाँचा |
| 5. | प्रस्तर युग : आदिम मानव |
| 6. | ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ |
| 7. | हड़प्पा संस्कृतिः कांस्य युग सभ्यता |
| 8. | आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग |
| 9. | उत्तर वैदिक अवस्था: राज्य और वर्ण व्यवस्था कीओर |
| 10. | जैन और बौद्ध धर्म |
अध्याय 1: प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्त्व
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- प्राचीन भारतीय इतिहास भारत की संस्कृति, परंपराओं, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक जड़ों को समझने में मदद करता है।
- यह हमें यह जानने में सहायता करता है कि वर्तमान भारतीय समाज, इसकी संस्थाएँ और इसकी चुनौतियाँ कैसे विकसित हुईं।
- इतिहास केवल घटनाओं की सूची नहीं है, बल्कि यह अतीत के अनुभवों से सीखने का एक साधन है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
| आस्पेक्ट | महत्त्व |
|---|---|
| सांस्कृतिक विरासत | भारतीय कला, धर्म, साहित्य और स्थापत्य कला का विकास समझने में मदद करता है। |
| राजनीतिक विकास | विभिन्न शासकों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, राज्य संरचनाओं और राजतंत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। |
| सामाजिक संरचना | जाति व्यवस्था, जेंडर संबंध, सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक सुधारों का अध्ययन। |
| आर्थिक गतिविधियाँ | कृषि, व्यापार, शिल्प और राजस्व व्यवस्था की ऐतिहासिक पड़ताल। |
| वैज्ञानिक एवं तकनीकी योगदान | गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा आदि में भारत के योगदान को उजागर करता है। |
| राष्ट्रीय एकता एवं पहचान | राष्ट्रवाद और स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक घटनाओं की भूमिका। |
इतिहास के स्रोत
(क) पुरातात्त्विक स्रोत
| स्रोत | उदाहरण |
|---|---|
| अवशेष | सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, स्थलों की खुदाई। |
| शिलालेख | अशोक के अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति (हर्षवर्धन), इलाहाबाद शिलालेख। |
| मुद्राएँ | गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राएँ, मौर्य कालीन पंचमार्क सिक्के। |
| स्मारक और मंदिर | अजंता-एलोरा की गुफाएँ, कोणार्क मंदिर, खजुराहो मंदिर। |
(ख) साहित्यिक स्रोत
| प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| धार्मिक ग्रंथ | वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण। |
| अधार्मिक ग्रंथ | अर्थशास्त्र (चाणक्य), राजा तरंगिणी (कल्हण), नाट्यशास्त्र (भरत मुनि)। |
| जातीय इतिहास | राजतरंगिणी, पुराण, तमिल संगम साहित्य। |
(ग) विदेशी स्रोत
| विदेशी यात्री | कृतियाँ |
|---|---|
| मेगास्थनीज | ‘इंडिका’ (चंद्रगुप्त मौर्य के समय)। |
| फाह्यान | गुप्त काल के दौरान भारत यात्रा। |
| ह्वेनसांग | हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा। |
| अल-बरूनी | ‘तहकीक-ए-हिंद’ (11वीं शताब्दी)। |
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | मुख्य विचारधारा | प्रमुख इतिहासकार |
|---|---|---|
| औपनिवेशिक | भारत को पिछड़ा और अयोग्य दिखाना | जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ |
| राष्ट्रवादी | भारतीय गौरव और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रमुखता देना | आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर |
| मार्क्सवादी | आर्थिक और वर्ग संघर्ष पर बल | डी.डी. कोशांबी, रोमिला थापर |
| नव-व्याख्यात्मक (Subaltern) | आम लोगों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों का अध्ययन | रणजीत गुहा, बिपिन चंद्र |
| संस्कृतिवादी | भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को आधार बनाना | के.एम. मुंशी |
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| पुरातत्व | भूतकाल की वस्तुओं, इमारतों और अवशेषों का अध्ययन। |
| शिलालेख | पत्थरों या धातुओं पर खुदे हुए ऐतिहासिक लेख। |
| इतिहास लेखन | अतीत के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियाँ। |
| सांस्कृतिक अधिग्रहण | एक सभ्यता द्वारा दूसरी सभ्यता से ज्ञान ग्रहण करना। |
| जातीय अध्ययन | विभिन्न जातीय समूहों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की खोज। |
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| तिथि / कालखंड | घटना |
|---|---|
| 6000 ई.पू. | प्रथम कृषि समुदायों का उदय। |
| 2500-1900 ई.पू. | सिंधु घाटी सभ्यता का उत्कर्ष। |
| 600 ई.पू. | महाजनपदों का उदय। |
| 322-185 ई.पू. | मौर्य साम्राज्य। |
| 78 ई. | शक संवत का प्रारंभ। |
| 320-550 ई. | गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। |
| 712 ई. | मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण। |
संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन वर्तमान समाज, संस्कृति और राजनीति को समझने के लिए आवश्यक है।
- विभिन्न स्रोतों – पुरातात्त्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों – से हमें अतीत की जानकारी मिलती है।
- इतिहास लेखन के औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और अन्य दृष्टिकोणों ने इतिहास की व्याख्या को अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है।
- यह अध्ययन UPSC परीक्षा के लिए न केवल सामान्य अध्ययन बल्कि निबंध और वैकल्पिक विषय (इतिहास) में भी सहायक है।
UPSC के लिए उपयोगिता
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):
- स्रोत, विदेशी यात्री, तिथियाँ, घटनाएँ, प्रमुख ग्रंथ।
- महत्वपूर्ण साम्राज्यों और उनके योगदान पर प्रश्न।
मुख्य परीक्षा (Mains):
- समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और संस्कृति पर आधारित प्रश्न।
- इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण।
- भारतीय इतिहास में राष्ट्रीयता और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका।
सुझाव:
- इसे बार-बार पढ़ें और मुख्य बिंदुओं को कवर करें।
- टेबल और चार्ट से समझने की कोशिश करें।
- प्रमुख तिथियों और स्रोतों को याद रखें।
यह UPSC के लिए अत्यंत उपयोगी नोट्स हैं। अगर किसी और विषय पर गहराई से चर्चा करनी हो तो बताएं! 😊📖→तुर्क आदि अनेक प्रजातियाँ शामिल थीं। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आपस में इस तरह नीरक्षीरवत् हो गए कि आज उनमें से किसी को भी उनके मूल रूप से साफ-साफ पहचा नहीं सकते हैं।
अध्याय 2: प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।
- इतिहास के स्रोतों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने विश्लेषण किया है।
- औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी एवं अन्य दृष्टिकोणों के आधार पर इतिहास की व्याख्या भिन्न-भिन्न हुई है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- संस्कृति और परंपराओं की समझ: भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को समझने में सहायक।
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास: शासन व्यवस्था और नीतियों का विश्लेषण।
- आर्थिक विकास: कृषि, व्यापार, और वाणिज्यिक गतिविधियों का अध्ययन।
- सामाजिक संरचना: वर्ण व्यवस्था, जाति प्रणाली और समाज में आए परिवर्तनों का अध्ययन।
- विदेशी प्रभाव: भारत पर विदेशी शासकों और यात्रियों के प्रभाव का आकलन।
इतिहास के स्रोत
(i) पुरातात्त्विक स्रोत
- अवशेष: स्थलों की खुदाई से प्राप्त मंदिर, स्तूप, दुर्ग आदि।
- शिलालेख: अशोक, समुद्रगुप्त आदि के अभिलेख।
- मुद्राएँ: शासकों की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।
- अभिलेख: ताम्रपत्र, राजपत्र आदि।
(ii) साहित्यिक स्रोत
- धार्मिक ग्रंथ: वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ।
- गैर-धार्मिक ग्रंथ: अर्थशास्त्र (कौटिल्य), राजतरंगिणी (कल्हण)।
- नाट्य और काव्य: कालिदास, भास, विष्णु शर्मा के ग्रंथ।
(iii) विदेशी स्रोत
- यूनानी और रोमन: मेगस्थनीज (इंडिका), टॉलेमी।
- चीनी यात्री: फाह्यान, ह्वेनसांग।
- अरबी और फारसी स्रोत: अल-बरूनी, इब्न बतूता।
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
(i) औपनिवेशिक दृष्टिकोण
- ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया।
- जेम्स मिल ने भारत को तीन कालों (हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश) में विभाजित किया।
(ii) राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
- भारतीय विद्वानों ने गौरवशाली अतीत को उजागर किया।
- आर.सी. मजूमदार, के.पी. जयस्वाल प्रमुख लेखक।
(iii) मार्क्सवादी दृष्टिकोण
- उत्पादन संबंधों और वर्ग संघर्ष पर केंद्रित अध्ययन।
- डी.डी. कोशांबी, रोमिला थापर प्रमुख विद्वान।
(iv) सांस्कृतिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
- भारतीय संस्कृति और परंपराओं को महत्व दिया गया।
- बल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष प्रमुख लेखक।
(v) उपनिवेश-विरोधी दृष्टिकोण
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इतिहास का अध्ययन।
- बिपिन चंद्र, सुमित सरकार प्रमुख विद्वान।
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| पुरातत्त्व | भौतिक अवशेषों का अध्ययन |
| अभिलेख | ताम्रपत्र, शिलालेख आदि |
| ऐतिहासिक स्रोत | पुरातात्त्विक, साहित्यिक, विदेशी स्रोत |
| मार्क्सवादी इतिहास लेखन | उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष आधारित अध्ययन |
| राष्ट्रवादी इतिहास लेखन | भारत के गौरवशाली अतीत पर बल |
| औपनिवेशिक दृष्टिकोण | ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया इतिहास लेखन |
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| वर्ष | घटना |
| 321 ईसा पूर्व | मौर्य साम्राज्य की स्थापना |
| 78 ईस्वी | शक संवत की शुरुआत |
| 4-5वीं सदी | गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष |
| 1206 | दिल्ली सल्तनत की स्थापना |
| 1526 | मुग़ल साम्राज्य की नींव |
| 1757 | प्लासी का युद्ध और ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत |
संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्त्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोत उपलब्ध हैं।
- विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर इतिहास लेखन में विविधता देखी जाती है।
- इतिहासकारों के दृष्टिकोण समय और संदर्भ के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।
- UPSC के लिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहास लेखन की पद्धति को समझने में मदद करता है।
अध्याय 3: स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- इतिहास का अध्ययन विभिन्न स्रोतों पर आधारित होता है।
- प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए पुरातात्त्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोतों का सहारा लिया जाता है।
- इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियाँ समय के साथ विकसित हुई हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है।
- सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं का विश्लेषण करने में सहायक।
- ऐतिहासिक घटनाओं से वर्तमान की नीतियों और समाज पर प्रभाव का आकलन।
इतिहास के स्रोत
(क) पुरातात्त्विक स्रोत
| स्रोत | उदाहरण |
|---|---|
| अभिलेख (Inscriptions) | अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति |
| मुद्राएँ (Coins) | गुप्त, कुषाण व सातवाहन राजवंशों की मुद्राएँ |
| स्मारक व स्थापत्य | मोहनजोदड़ो, हरप्पा, अजन्ता-एलोरा गुफाएँ |
| उपकरण व अस्त्र-शस्त्र | ताम्रपाषाण कालीन उपकरण |
(ख) साहित्यिक स्रोत
| प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| धार्मिक ग्रंथ | वेद, पुराण, जैन और बौद्ध साहित्य |
| ऐतिहासिक ग्रंथ | राजतरंगिणी (कल्हण), हरषचरित (बाणभट्ट) |
| महाकाव्य | रामायण, महाभारत |
| तमिल संगम साहित्य | शिलप्पदिकारम, मणिमेखलै |
(ग) विदेशी यात्रियों के विवरण
| यात्री | काल | रचना |
|---|---|---|
| मेगस्थनीज | चंद्रगुप्त मौर्य | इंडिका |
| फाह्यान | गुप्त काल | फो-गुओ-जी |
| ह्वेनसांग | हर्षवर्धन काल | सी-यू-की |
| अलबरूनी | महमूद गजनी | किताब-उल-हिंद |
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | प्रमुख विचारक | विशेषताएँ |
|---|---|---|
| औपनिवेशिक | विलियम जोन्स, जेम्स मिल | भारतीय इतिहास को यूरोपीय नजरिए से देखा |
| राष्ट्रवादी | आर.सी. मजूमदार, के.पी. जयस्वाल | गौरवशाली भारतीय अतीत पर बल |
| मार्क्सवादी | डी.डी. कोसांबी, आर.एस. शर्मा | आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान |
| उपनिवेश-विरोधी | सुबAlternateern स्टडीज़ समूह | इतिहास में आम जन और हाशिए के समूहों का समावेश |
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
- पुरातत्त्वविद्या: भौतिक अवशेषों के अध्ययन द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण।
- एपिग्राफी: अभिलेखों (शिलालेखों) का अध्ययन।
- न्यूमिस्मेटिक्स: सिक्कों का अध्ययन।
- इतिहास लेखन: विभिन्न स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं का विश्लेषण।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 326 ई.पू. | सिकंदर का भारत अभियान |
| 273-232 ई.पू. | अशोक का शासनकाल और शिलालेख |
| 399-414 ई. | फाह्यान की भारत यात्रा |
| 1017-1030 ई. | अलबरूनी का भारत आगमन |
संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- प्राचीन भारतीय इतिहास विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, जिनमें पुरातात्त्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्रमुख हैं।
- इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जो समय के साथ बदलते गए।
- इतिहास को समझने के लिए स्रोतों की सत्यता और विश्लेषण आवश्यक है।
- UPSC परीक्षा के लिए इन स्रोतों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि यह प्राचीन भारत के मूलभूत तथ्यों को स्पष्ट करता है।
अध्याय 4: भौगोलिक ढाँचा – विस्तृत नोट्स (UPSC हेतु)
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- भारत का भौगोलिक ढाँचा उसके इतिहास, समाज और संस्कृति को प्रभावित करता है।
- प्राचीन काल से ही विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को दिशा दी।
- नदियाँ, पर्वत, जलवायु और अन्य भौगोलिक तत्व भारत की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को समझने में सहायक।
- ऐतिहासिक घटनाओं के मूल कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करने में सहायक।
- प्रशासनिक नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायक।
इतिहास के स्रोत
| स्रोत का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| पुरातात्त्विक स्रोत | स्थलों की खुदाई, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, चित्रित पात्र आदि। |
| साहित्यिक स्रोत | वेद, पुराण, महाकाव्य (रामायण, महाभारत), जैन-बौद्ध साहित्य, तमिल संगम साहित्य। |
| विदेशी विवरण | मेगस्थनीज (इंडिका), फाह्यान, ह्वेनसांग, अलबरूनी आदि के यात्रा विवरण। |
| मौखिक स्रोत | लोककथाएँ, किंवदंतियाँ, गीत, लोकसाहित्य। |
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | प्रमुख विचार |
|---|---|
| औपनिवेशिक | ब्रिटिश इतिहासकारों का दृष्टिकोण, भारतीय समाज को स्थिर और अविकसित बताने की प्रवृत्ति। |
| राष्ट्रवादी | भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित, भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करने वाला। |
| मार्क्सवादी | वर्ग-संघर्ष, आर्थिक संरचना, समाज की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण करता है। |
| सांस्कृतिक | भारत की सांस्कृतिक एकता और धार्मिक परंपराओं पर केंद्रित। |
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
- स्थलाकृतिक विशेषताएँ: पर्वत, पठार, नदियाँ, समुद्र तट आदि।
- मानव-भूगोल: जलवायु, कृषि, वनस्पति, जनसंख्या आदि का अध्ययन।
- नदी घाटी सभ्यता: सिंधु घाटी सभ्यता जैसी प्राचीन सभ्यताओं का विश्लेषण।
- प्लेट विवर्तनिकी: महाद्वीपीय प्रवाह और भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| वर्ष/काल | घटना |
|---|---|
| लगभग 7000 ईसा पूर्व | प्रारंभिक कृषि और बस्तियों की स्थापना। |
| लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व | सिंधु घाटी सभ्यता का उत्कर्ष। |
| लगभग 1500 ईसा पूर्व | आर्यों का आगमन और वैदिक संस्कृति का विकास। |
| लगभग 600 ईसा पूर्व | महाजनपदों का उदय और बौद्ध-जैन परंपराओं का प्रसार। |
| लगभग 300 ईसा पूर्व | मौर्य साम्राज्य का गठन। |
संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- भारत का भौगोलिक ढाँचा ऐतिहासिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक रहा है।
- नदियों ने कृषि और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पर्वत श्रृंखलाओं ने सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया।
- समुद्र तटों ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में योगदान दिया।
- ऐतिहासिक दृष्टिकोणों की विविधता से भारत के इतिहास की बहुआयामी समझ बनती है।
निष्कर्ष: भौगोलिक कारकों की भूमिका भारतीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण रही है। यह न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करता है, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को भी दिशा प्रदान करता है।
अध्याय 5: प्रस्तर युग एवं आदिम मानव (Old NCERT – R.S. Sharma, अध्याय 5)
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- प्रस्तर युग मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण है, जब मनुष्य पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था।
- इसे मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है:
- पुरापाषाण युग (Paleolithic Age)
- मध्यपाषाण युग (Mesolithic Age)
- नवपाषाण युग (Neolithic Age)
- इस युग की जानकारी पुरातात्त्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें औजार, गुफा चित्र और हड्डियों के अवशेष शामिल हैं।
- यह युग मानव विकास और समाज की उत्पत्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- भारत के अतीत को समझने और वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को जानने के लिए।
- ऐतिहासिक घटनाओं और सभ्यताओं के उदय-पतन का अध्ययन करने के लिए।
- मानव विकास की प्रक्रिया, कृषि की शुरुआत, और स्थायी बस्तियों के विकास को समझने में सहायक।
- प्रशासनिक, आर्थिक, और धार्मिक गतिविधियों के विकास का आकलन।
इतिहास के स्रोत
(A) पुरातात्त्विक स्रोत
- प्रस्तर औजार, मिट्टी के बर्तन, हड्डियाँ, गुफा चित्र, पुरानी बस्तियाँ।
- खुदाई से प्राप्त स्थल जैसे भीमबेटका, आदमगढ़, बेलन घाटी आदि।
(B) साहित्यिक स्रोत
- वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जातक कथाएँ।
- बौद्ध और जैन ग्रंथ जैसे त्रिपिटक और अँगुत्तर निकाय।
(C) विदेशी स्रोत
- यूनानी, रोमन, चीनी यात्रियों के विवरण।
- हेरोडोटस, टॉलेमी, फाह्यान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत।
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | प्रमुख विचार |
|---|---|
| औपनिवेशिक | भारतीय इतिहास को ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से देखा गया। |
| राष्ट्रवादी | भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गौरवशाली विरासत को दर्शाता है। |
| मार्क्सवादी | आर्थिक और सामाजिक संरचना पर बल देता है। |
| उपनिवेशोत्तर | भारतीय इतिहास की व्याख्या भारतीय दृष्टिकोण से करता है। |
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
- पुरापाषाण युग: मानव इतिहास का सबसे पुराना चरण, जिसमें पत्थर के असभ्य औजारों का प्रयोग होता था।
- मध्यपाषाण युग: छोटे पत्थर के औजारों (Microliths) का उपयोग शुरू हुआ।
- नवपाषाण युग: कृषि, स्थायी बस्तियाँ और पशुपालन का विकास हुआ।
- हड़प्पा सभ्यता: सिंधु घाटी सभ्यता, जो नवपाषाण काल के बाद विकसित हुई।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| तिथि (लगभग) | घटना |
|---|---|
| 20 लाख वर्ष पूर्व | मानव के प्रारंभिक अवशेष अफ्रीका में मिले। |
| 2 लाख वर्ष पूर्व | होमो सेपियंस का विकास। |
| 10,000 ईसा पूर्व | नवपाषाण क्रांति की शुरुआत। |
| 2600-1900 ईसा पूर्व | हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल। |
संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- प्रस्तर युग मानव इतिहास का प्रारंभिक चरण था, जिसमें उपकरणों के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था।
- धीरे-धीरे मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और स्थायी निवास की ओर बढ़ा।
- इतिहास को विभिन्न स्रोतों से समझा जाता है, जिनमें पुरातात्त्विक और साहित्यिक स्रोत प्रमुख हैं।
- इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण शामिल हैं।
- इस युग का अध्ययन हमें सभ्यता के विकास और मानव समाज की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है।
यह नोट्स UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी हैं और प्रस्तर युग को समझने में सहायक सिद्ध होंगे।
अध्याय 6: ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- ताम्रपाषाण युग (Chalcolithic Age) भारत में तांबे और पत्थर के उपकरणों के संयुक्त उपयोग का युग था।
- यह लगभग 2500-700 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में रहा।
- इस युग की विशेषता कृषि आधारित जीवन शैली, बस्तियों की स्थापना और मिट्टी के बर्तनों का विकास था।
- यह संस्कृति हड़प्पा सभ्यता और लौह युग के मध्य की कड़ी मानी जाती है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को समझने में सहायक।
- कृषि और स्थायी बस्तियों की उत्पत्ति का अध्ययन।
- क्षेत्रीय संस्कृतियों और उनके प्रभावों का विश्लेषण।
- आधुनिक भारतीय समाज में ऐतिहासिक परंपराओं का प्रभाव।
इतिहास के स्रोत
(क) पुरातात्त्विक स्रोत
- स्थल: इनामगाँव, कायथा, एरण, नागदा, आम्बेरी, आदि।
- उपकरण: तांबे के औजार, पत्थर के औजार, आभूषण।
- मिट्टी के बर्तन: लाल, काले और चित्रित मृदभांड।
- मकान: कच्ची ईंट और मिट्टी के घर।
- अनाज: गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, दालें।
(ख) साहित्यिक स्रोत
- वैदिक साहित्य में कृषि और बस्तियों का वर्णन।
- संस्कृत, प्राकृत और तमिल साहित्य में संदर्भ।
(ग) विदेशी स्रोत
- ग्रीक, चीनी और अरबी यात्रियों के लेख।
- टॉलेमी एवं प्लिनी के वर्णन।
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | विशेषताएँ |
|---|---|
| मार्क्सवादी | आर्थिक संरचना, वर्ग संघर्ष पर बल |
| राष्ट्रवादी | गौरवशाली अतीत को उजागर करना |
| औपनिवेशिक | भारत को पश्चिमी दृष्टि से देखना |
| नव-इतिहासलेखन | बहुआयामी अध्ययन (पुरातत्व, नृविज्ञान) |
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
- ताम्रपाषाण: तांबे और पत्थर के उपकरणों का युग।
- मृदभांड: मिट्टी के बर्तन, जिनमें चित्रित और साधारण दोनों शामिल।
- बस्तियाँ: स्थायी आवास जिनमें घर, कुएँ, अनाज रखने के स्थान थे।
- खाद्य उत्पादन: गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मांसाहार आदि।
- आभूषण: तांबे, मिट्टी, हड्डी और मनकों से निर्मित।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| वर्ष (ईसा पूर्व) | घटना |
|---|---|
| 2500-2000 | ताम्रपाषाण संस्कृतियों का विकास |
| 1800-1000 | स्थायी बस्तियों का उन्नयन |
| 1000-700 | लौह युग की ओर संक्रमण |
7. संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- ताम्रपाषाण काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन युग था।
- इस युग में कृषि, बस्तियों और मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ।
- ताम्रपाषाण संस्कृतियों की जानकारी पुरातात्त्विक स्थलों से प्राप्त होती है।
- यह काल भविष्य में लौह युग और महाजनपदों के विकास का आधार बना।
निष्कर्ष: ताम्रपाषाण युग भारतीय इतिहास में कृषि-आधारित स्थायी बस्तियों की शुरुआत का प्रतीक है। इस युग की संस्कृतियाँ हमें प्राचीन भारतीय समाज, उसकी आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक विकास को समझने में मदद करती हैं।
अध्याय 7: हज़प्पा संस्कृतिः कांस्य युग सभ्यता
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- हड़प्पा सभ्यता (सिंधु घाटी सभ्यता) विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी।
- इसका काल 2500-1750 ईसा पूर्व माना जाता है।
- यह कांस्य युग की एक विकसित नगरीय सभ्यता थी।
- इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी (हड़प्पा) और 1922 में आर. डी. बनर्जी (मोहनजोदड़ो) ने की।
- यह मुख्यतः पाकिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक फैली थी।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समझने में मदद करता है।
- समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म की उत्पत्ति व विकास की जानकारी देता है।
- भारत की प्राचीन सभ्यताओं और अन्य समकालीन सभ्यताओं के बीच तुलना करने में सहायक।
- आधुनिक राष्ट्र निर्माण में इसकी ऐतिहासिक भूमिका।
इतिहास के स्रोत
| स्रोत | विवरण |
|---|---|
| पुरातात्त्विक स्रोत | स्थलों की खुदाई, मुद्राएँ, मूर्तियाँ, भवन, औजार, अवशेष |
| साहित्यिक स्रोत | वैदिक साहित्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ, महाकाव्य (रामायण, महाभारत) |
| विदेशी स्रोत | यूनानी, चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत (मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग) |
| शिलालेख व अभिलेख | अशोक के शिलालेख, मुद्राएँ, ताम्रपत्र |
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|
| औपनिवेशिक दृष्टिकोण | भारत को पिछड़ा दिखाना, यूरोपीय श्रेष्ठता सिद्ध करना |
| राष्ट्रवादी दृष्टिकोण | भारत के गौरवशाली अतीत पर बल, प्राचीन संस्कृति का उत्थान |
| मार्क्सवादी दृष्टिकोण | वर्ग संघर्ष, आर्थिक पहलुओं पर बल, समाज के वर्ग विभाजन की व्याख्या |
| परंपरागत दृष्टिकोण | धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों को अधिक महत्त्व देना |
हड़प्पा सभ्यता के मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
| कीवर्ड | परिभाषा |
|---|---|
| नगरीय सभ्यता | नियोजित नगरों, सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली वाली सभ्यता |
| ग्रेट बाथ | मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल जलाशय, संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए |
| लिपि | हड़प्पाई लिपि अभी तक अपठित |
| ड्रैविड़ियन परिकल्पना | माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ भाषा-भाषी थे |
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1921 | दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की |
| 1922 | आर. डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की |
| 1953 | अमरीका के जॉर्ज डेल्स ने जल-प्रलय सिद्धांत प्रस्तुत किया |
| 1964 | हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण हेतु रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग |
हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त सारांश
- नगर नियोजन: सड़कें सीधी व समकोण पर, जल निकासी प्रणाली विकसित।
- आर्थिक व्यवस्था: कृषि (गेहूँ, जौ), पशुपालन, व्यापार (मेसोपोटामिया से)।
- धार्मिक जीवन: मातृदेवी पूजा, पशुपति महादेव की अवधारणा।
- लिपि व कला: चित्रलिपि (अभी तक अपठित), टेराकोटा, मूर्तियाँ, मुहरें।
- हड़प्पा सभ्यता का पतन: जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्यों का आगमन, आंतरिक कारण।
निष्कर्ष
- हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम उन्नत सभ्यताओं में से एक थी।
- यह नगर नियोजन, कला, व्यापार, और सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक विकसित थी।
- इसके पतन के कारण बहु-आयामी थे और इस पर अभी भी शोध जारी है।
- इसकी खोज और अध्ययन से भारतीय इतिहास को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है।
UPSC परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्यों का सार:
- सबसे बड़ा स्थल: राखीगढ़ी (हरियाणा)
- सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम: हड़प्पा सभ्यता
- मुख्य बंदरगाह: लोथल (गुजरात)
- सभ्यता की भाषा: अज्ञात (हड़प्पाई लिपि)
ये नोट्स UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे।
अध्याय 8: आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- यह अध्याय प्राचीन भारत में आर्यों के आगमन और ऋग्वैदिक समाज की संरचना का अध्ययन करता है।
- आर्यों के मूल स्थान, उनके आगमन की प्रक्रिया, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक विचारधारा और उनके प्रभावों पर चर्चा की गई है।
- ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो इस युग की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- भारतीय सभ्यता के उद्भव और विकास को समझने में सहायक।
- समाज की संरचना, आर्थिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक विकास का विश्लेषण।
- विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं की पुनर्व्याख्या।
- भारतीय समाज में धर्म, जाति, भाषा और रीति-रिवाजों की उत्पत्ति को समझने में सहायक।
इतिहास के स्रोत
(क) पुरातात्त्विक स्रोत
- उत्खनन स्थल: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन।
- मुद्राएँ और अभिलेख: अशोक के शिलालेख, सिक्के।
- भवन अवशेष: वेदिक सभ्यता के दौरान प्राप्त यज्ञ वेदियाँ।
(ख) साहित्यिक स्रोत
- वैदिक साहित्य: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
- ब्राह्मण ग्रंथ: शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण।
- उपनिषद और महाकाव्य: भगवद गीता, महाभारत, रामायण।
(ग) विदेशी स्रोत
- ग्रीक लेखक: हेरोडोटस, टॉलमी।
- चीनी यात्री: फाह्यान, ह्वेनसांग।
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|
| मार्क्सवादी | आर्थिक और वर्ग संघर्ष पर केंद्रित, डी. डी. कोसांबी द्वारा प्रवर्तित |
| राष्ट्रवादी | भारतीय संस्कृति और गौरव को महत्त्व दिया, आर. सी. मजूमदार द्वारा समर्थित |
| औपनिवेशिक | यूरोपीय दृष्टिकोण, भारतीय समाज को पिछड़ा बताने की प्रवृत्ति |
| पारंपरिक | धार्मिक ग्रंथों को ऐतिहासिक स्रोत मानकर अध्ययन |
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
- आर्य: एक जातीय समूह, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन किया।
- ऋग्वेद: सबसे पुराना वेद, जिसमें 1028 ऋचाएँ हैं।
- कुल/ग्राम: सामाजिक इकाई, जिसका नेतृत्व कुलपति करता था।
- सभा और समिति: जनतांत्रिक संस्थाएँ, जो प्रशासनिक निर्णयों में सहायक थीं।
- गोत्र: कुल की पहचान, वैवाहिक संबंधों का आधार।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| तिथि/काल | घटना |
|---|---|
| 1500-1000 ई.पू. | आर्यों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन |
| 1200-1000 ई.पू. | प्रारंभिक वैदिक काल (ऋग्वैदिक युग) |
| 1000-600 ई.पू. | उत्तर वैदिक काल |
| 600 ई.पू. | महाजनपदों का उदय |
संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- आर्यों का आगमन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय सभ्यता को नया रूप दिया।
- ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि यह समाज मुख्यतः पशुपालक एवं कृषि-आधारित था।
- राजनीतिक व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, जिसमें राजा के निर्णयों में सभा और समिति की भूमिका थी।
- धर्म में प्रकृति पूजा का महत्त्व था और यज्ञ अनुष्ठानों की परंपरा थी।
- यह काल भारतीय समाज की संरचना और सांस्कृतिक विकास के लिए आधारभूत था।
निष्कर्ष:
ऋग्वैदिक युग भारतीय समाज की आधारशिला थी, जिसने आगे चलकर उत्तर वैदिक काल और महाजनपदों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस काल का अध्ययन न केवल प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में सहायक है, बल्कि वर्तमान भारतीय समाज के मूलभूत तत्त्वों को भी स्पष्ट करता है।
अध्याय 8:उत्तर वैदिक अवस्था: राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
उत्तर वैदिक काल (1000-600 ईसा पूर्व) भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में जनजातीय समाज से संगठित राज्य की ओर परिवर्तन हुआ और वर्ण व्यवस्था अधिक सुस्पष्ट हुई। कृषि, लोहे के उपयोग और नगरों के विकास के साथ सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनाओं में गहरे परिवर्तन हुए।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उत्पत्ति और विकास को समझने में सहायक।
- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकास की जानकारी प्रदान करता है।
- आधुनिक प्रशासन, संविधान और सामाजिक संरचनाओं को समझने में मदद करता है।
- UPSC जैसे परीक्षाओं के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करता है।
इतिहास के स्रोत
1. पुरातात्त्विक स्रोत
- लोहे के उपकरण और कृषि औजार (उत्तर वैदिक काल की विशेषता)
- चित्रित धूसर मृदभांड (PGW) संस्कृति के अवशेष
- बसावटों और किलेबंद नगरों के प्रमाण (कौशांबी, हस्तिनापुर)
2. साहित्यिक स्रोत
- उत्तर वैदिक ग्रंथ: सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद
- ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद
- महाकाव्य: रामायण और महाभारत
- सूत्र ग्रंथ: श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र
3. विदेशी स्रोत
- ग्रीक और चीनी यात्रियों (मेगस्थनीज, फाह्यान) के विवरण
इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | विशेषताएँ |
|---|---|
| औपनिवेशिक | भारतीय समाज को विभाजित करने और यूरोपीय श्रेष्ठता सिद्ध करने पर जोर |
| राष्ट्रवादी | वैदिक संस्कृति को गौरवशाली बताने और भारतीय परंपराओं को महत्त्व देने पर जोर |
| मार्क्सवादी | समाज और राज्य की उत्पत्ति को आर्थिक वर्ग-संघर्ष और उत्पादन साधनों के नियंत्रण से जोड़ना |
| पारंपरिक | धार्मिक ग्रंथों को ऐतिहासिक स्रोत मानना |
मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
जनपद: छोटे राजनीतिक इकाइयाँ
- महाजनपद: बड़े और संगठित जनपद (16 महाजनपदों का उल्लेख)
- राजसूय यज्ञ: राजा की शक्ति का प्रदर्शन करने वाला यज्ञ
- वर्ण व्यवस्था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सामाजिक श्रेणियाँ
- गृहस्थाश्रम: सामाजिक जीवन के चार आश्रमों में से एक (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास)
- श्रमण परंपरा: जैन और बौद्ध संप्रदायों की धार्मिक धारा
महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| तिथि/काल | घटना |
|---|---|
| 1000-600 BCE | उत्तर वैदिक काल |
| 800-600 BCE | उपनिषदों की रचना |
| 600 BCE | महाजनपद काल की शुरुआत |
संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। कृषि और व्यापार की प्रगति के कारण जनजातीय व्यवस्था समाप्त होकर संगठित राज्य की स्थापना हुई। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभाव बढ़ा। इस काल में बौद्ध और जैन धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
निष्कर्ष: यह काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आगे चलकर महाजनपदों और प्रारंभिक राज्यों की नींव रखी।
अध्याय 10: जैन और बौद्ध धर्म (Old NCERT R S Sharma)
1. अध्याय का संक्षिप्त परिचय
- जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई।
- दोनों धर्मों ने वैदिक परंपराओं और कर्मकांडों का विरोध किया।
- इनका उदय सामाजिक और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता से हुआ।
- अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर आधारित हैं।
- इनका प्रभाव भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर व्यापक रूप से पड़ा।
2. प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्त्व
- भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को समझने में सहायक।
- धार्मिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं का विकास।
- जाति प्रथा, समाज सुधार और अन्य सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन।
- वैश्विक दृष्टिकोण से भारतीय सभ्यता की भूमिका।
3. इतिहास के स्रोत
(i) पुरातात्त्विक स्रोत
- स्तूप (सांची, अमरावती, भरहुत)
- अभिलेख (अशोक के शिलालेख)
- मूर्तिकला और स्थापत्य कला
- सिक्के और मुद्रा विज्ञान
(ii) साहित्यिक स्रोत
- त्रिपिटक (बौद्ध धर्म के ग्रंथ)
- जैन आगम (जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ)
- महावंश और दीपवंश (श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ)
(iii) विदेशी स्रोत
- मेगस्थनीज की ‘इंडिका’
- फाह्यान और ह्वेनसांग की यात्राएं
4. इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण
| दृष्टिकोण | प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|
| मार्क्सवादी | आर्थिक और सामाजिक संरचना पर जोर, वर्ग संघर्ष का विश्लेषण |
| राष्ट्रवादी | भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता पर केंद्रित |
| औपनिवेशिक | यूरोपीय दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की व्याख्या |
| अधुनिक दृष्टिकोण | बहुआयामी अध्ययन, विभिन्न स्रोतों का उपयोग |
5. मुख्य कीवर्ड और परिभाषाएँ
- तथागत – बुद्ध का एक नाम
- निर्वाण – जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति
- संघ – बौद्ध भिक्षुओं और जैन मुनियों का समूह
- अहिंसा – किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना
- षड्जीवनिका – जैन धर्म के 6 आवश्यक कर्तव्य
6. महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 563 ईसा पूर्व | गौतम बुद्ध का जन्म |
| 540 ईसा पूर्व | महावीर स्वामी का जन्म |
| 528 ईसा पूर्व | बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति (बोधगया) |
| 468 ईसा पूर्व | महावीर स्वामी का निर्वाण |
| 483 ईसा पूर्व | बुद्ध का महापरिनिर्वाण (कुशीनगर) |
| 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व | अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण |
| 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व | जैन आगमों का लेखन |
7. संक्षिप्त सारांश और निष्कर्ष
- जैन और बौद्ध धर्म ने समाज में नैतिकता, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया।
- कर्मकांडों और जाति-व्यवस्था के विरोध के कारण ये लोकप्रिय बने।
- बौद्ध धर्म को अशोक और कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया जिससे यह एशिया में फैल गया।
- जैन धर्म व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय रहा और गुजरात, राजस्थान में विशेष रूप से प्रभावी रहा।
- दोनों धर्मों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला।
- आज भी इनके सिद्धांतों का महत्त्व बना हुआ है।
Download – Click Here
ALSO READ – Old NCERT R S Sharma: Ancient History Notes For UPSC Hindi Part 2
ALSO READ –Old NCERT R S Sharma: Ancient History Notes For UPSC Hindi Part 3
ALSO READ – Ancient History Notes: UPSC NCERT Class 12th History Notes In Hindi Part 1
ALSO READ – UPSC NCERT Class 6th History Notes Hindi
FAQ-
(Q) मूर्ति पूजा का आरम्भ कब से माना जाता है?
Ans.-पूर्व आर्य काल से
(Q)मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है?
Ans.-मृतकों का टीला
(Q)सिंधु सभ्यता किससे सम्बंधित है?
Ans.-आद्य ऐतिहासिक युग (Proto-Historic Age) से
(Q) हड़प्पा सभ्यता की लिपि (Script) किस प्रकार थी?
Ans.-भावचित्रात्मक (Pictographic)
(Q)हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
Ans.-पुरातात्विक खुदाई